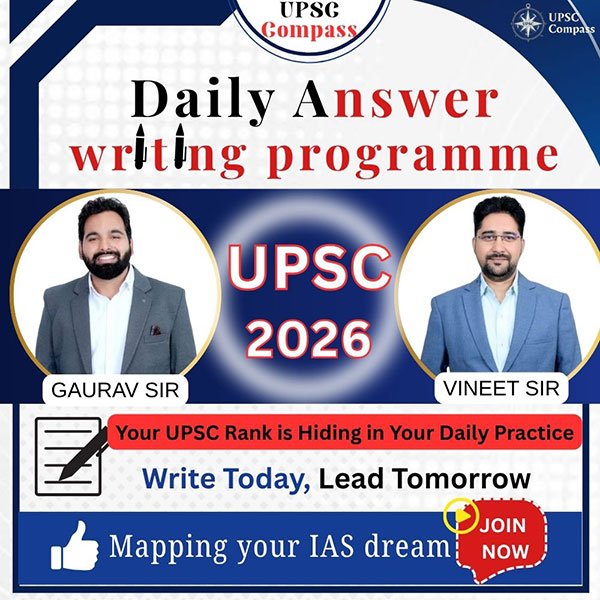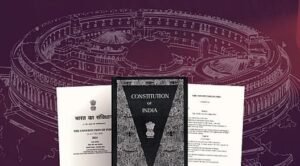
क्यों खबरों में?
-
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया है
-
इसमें प्रावधान है कि यदि मंत्री (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित) किसी गंभीर अपराध में, जिसकी सजा पाँच वर्ष या उससे अधिक है, 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा
विधेयक की मुख्य विशेषताएँ
-
दायरा
-
-
लागू होता है:
-
केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री)
-
राज्य सरकारें (राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री)
-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (मंत्री और मुख्यमंत्री)
-
-
अलग विधेयकों के माध्यम से पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित
-
-
हटाने के आधार
-
-
गंभीर अपराध – यदि किसी मंत्री पर पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का आरोप है
-
हिरासत प्रावधान – मंत्री को 30 लगातार दिनों तक न्यायिक हिरासत में होना चाहिए
-
हिरासत = न्यायालय द्वारा आदेशित कानूनी निरुद्ध या कैद; यह दोषसिद्धि (conviction) के समान नहीं है
-
-
हटाने की प्रक्रिया
-
-
केंद्रीय मंत्री – राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर (31वें दिन तक) हटाएँगे
-
राज्य मंत्री – राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर (31वें दिन तक) हटाएँगे
-
दिल्ली मंत्री – राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाएँगे
-
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री स्वयं – उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वे स्वतः पद से हटा दिए जाएँगे
-
-
पुनर्नियुक्ति
-
-
हटाना स्थायी अयोग्यता नहीं है
-
मंत्री रिहा होने के बाद पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं
-
प्रमुख प्रभाव
-
सकारात्मक पक्ष
-
-
संवैधानिक नैतिकता (ईमानदारी और संविधान के प्रति सम्मान) को मजबूत करने का प्रयास
-
सुशासन और जनविश्वास को बढ़ावा देता है, जिससे गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्री पद पर न रह सकें
-
-
नकारात्मक पक्ष
-
-
राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा, क्योंकि हटाना दोषसिद्धि पर नहीं बल्कि हिरासत पर आधारित है
-
लोकतांत्रिक मानदंड और सिद्धांत कमजोर हो सकते हैं
-
संवैधानिक और कानूनी मुद्दे
-
मूल संरचना का उल्लंघन
-
-
मूल संरचना सिद्धांत: केशवानंद भारती केस (1973) – संसद संविधान की मूल विशेषताओं (लोकतंत्र, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण) को नहीं बदल सकती
-
यह विधेयक संसदीय लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति अदालतों और विधानमंडल से हटकर कार्यपालिका के विवेक पर चली जाती है
-
-
न्यायिक परंपरा से विचलन
-
-
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 – अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद, न कि मुकदमे या हिरासत के दौरान
-
ए.आर. अंतुले केस (1988) – सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करने वाली प्रक्रियाओं को खारिज किया
-
-
कैबिनेट की सामूहिकता सिद्धांत का कमजोर होना
-
-
सामूहिकता = मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य करती है और उत्तरदायी होती है
-
हटाने की शक्ति केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर निर्भर होने से मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत विवेक की बंधक बन सकती है
-
एस.आर. बोम्मई केस (1994) – मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को संसदीय प्रणाली का हिस्सा बताया गया
-
-
जांच एजेंसियों के माध्यम से दुरुपयोग का खतरा
-
-
ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप
-
पीएमएलए जैसे कानूनों में जमानत बेहद कठिन (धारा 45 में कठोर शर्तें)
-
कई नेता दोषसिद्धि के बिना 30 दिन से अधिक हिरासत में रह सकते हैं, जिससे स्वतः हटाने का प्रावधान लागू होगा
-
-
स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया का ह्रास
-
-
न्यायिक प्रक्रिया = राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के सभी अधिकारों का सम्मान करना होगा
-
मेनका गांधी केस (1978) – स्वतंत्रता केवल न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत कानून से ही सीमित की जा सकती है
-
30 दिन की हिरासत का प्रावधान मनमाना है और मात्र जाँच को दोष के बराबर मानता है
-
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य
-
यूनाइटेड किंगडम
-
-
दोषसिद्धि तक इस्तीफे का कोई कानूनी दबाव नहीं
-
मंत्री अक्सर राजनीतिक दबाव या नैतिक कारणों से इस्तीफा देते हैं (प्रोफ्यूमो स्कैंडल, 1963)
-
-
संयुक्त राज्य अमेरिका
-
-
संविधान में मंत्रियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं
-
इस्तीफे आमतौर पर राजनीतिक दबाव से होते हैं (वाटरगेट स्कैंडल, 1974)
-
-
दक्षिण अफ्रीका
-
-
मंत्री केवल दोषसिद्धि या महाभियोग के बाद ही हटाए जा सकते हैं
-
यहाँ जवाबदेही के केंद्र में न्यायिक प्रक्रिया है
-
विधेयक के संभावित परिणाम
-
शासन अस्थिरता – बार-बार हटाए जाने से कैबिनेट की स्थिरता और नीतिगत निरंतरता प्रभावित
-
राजनीतिक हथियारकरण – सरकारें जाँच एजेंसियों का उपयोग प्रतिद्वंद्वियों को हटाने के लिए कर सकती हैं
-
जनादेश का ह्रास – दोषसिद्धि के बिना मतदाताओं की पसंद को पलट सकता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर होगा
-
न्यायिक बोझ – हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ेगी, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ेगा
-
नैतिक मानदंडों का जोखिम – जवाबदेही बढ़ाने की बजाय दुरुपयोग से राजनीति में नैतिकता पर अविश्वास पैदा हो सकता है
आगे का रास्ता
-
हटाने को न्यायिक मील के पत्थरों से जोड़ना – केवल तब जब अदालत आरोप तय करे, न कि मात्र हिरासत पर
-
न्यायिक निगरानी को मजबूत करना – उच्च न्यायालय हटाने के आदेश को कम समय (जैसे 7 दिन) में देखे
-
सामूहिकता की सुरक्षा – हटाना केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर निर्भर न होकर मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय से हो
-
राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना – एक स्वतंत्र निकाय (जैसे लोकपाल या एथिक्स कमीशन) ऐसे मामलों की समीक्षा करे ताकि राजनीतिक प्रतिशोध से बचा जा सके
-
स्वैच्छिक आचार संहिता को बढ़ावा – मंत्री नैतिक आधार पर स्वयं इस्तीफा दें (जैसे 1956 में रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था), न कि मजबूरी में कानूनी अयोग्यता से
निष्कर्ष
-
यह विधेयक एक वास्तविक चिंता को संबोधित करता है – गंभीर आपराधिक आरोप झेल रहे मंत्री शासन और जनविश्वास को नुकसान पहुँचाते हैं
-
लेकिन हिरासत को दोष के बराबर मानना कार्यपालिका के दुरुपयोग, न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन और लोकतंत्र को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है
-
एक संतुलित सुधार में जवाबदेही के साथ न्यायिक सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी मजबूत हो