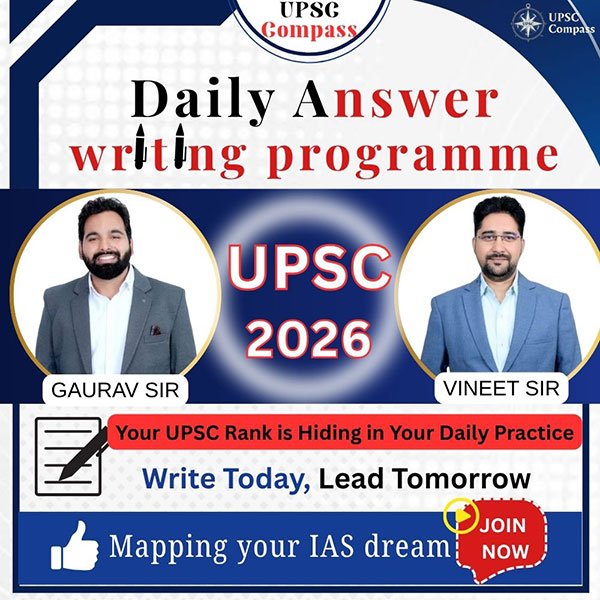समाचार में क्यों
-
मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया
-
ध्वनिमत से पारित होकर आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया
-
विपक्ष का कड़ा विरोध
-
आलोचकों ने इसे “असंवैधानिक,” “अलोकतांत्रिक,” और राजनीतिक दुरुपयोग का संभावित साधन बताया
-
-
उन मामलों से प्रेरित जहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे
-
उदाहरण: तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड
-
विधेयक का उद्देश्य
-
मंत्रियों (केंद्र और राज्य), जिनमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं, की जवाबदेही बढ़ाना
-
गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद पर बने रहने से रोकना
-
संवैधानिक नैतिकता, ईमानदारी और शासन में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
-
दायरा
-
-
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री
-
मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री
-
केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, जिनमें दिल्ली और जम्मू-कश्मीर शामिल
-
-
हटाने की प्रक्रिया
-
-
कोई मंत्री यदि 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य अपराध में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन स्वतः पद से हटा दिया जाएगा
-
हटाने का अधिकार
-
केंद्रीय मंत्री: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सीधे
-
राज्य मंत्री: राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर
-
मुख्यमंत्री: राज्यपाल सीधे
-
-
-
हिरासत, न कि दोषसिद्धि
-
-
हटाने का आधार हिरासत की अवधि है, न कि अदालत द्वारा दोषसिद्धि
-
रिहाई के बाद मंत्री को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, जिससे यह एक अस्थायी निवारक उपाय है
-
-
कानूनी संशोधन
-
-
अनुच्छेद 75 – प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री
-
अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री
-
अनुच्छेद 239AA – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके मंत्रियों का शासन
-
विधेयक की आवश्यकता
-
संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना
-
-
मंत्रियों से अपेक्षा है कि वे संदेह से परे हों और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखें
-
गिरफ्तार मंत्री यदि पद पर बने रहें तो संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुँच सकता है
-
-
संवैधानिक कमी को पूरा करना
-
-
वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है जो लंबे समय तक हिरासत में रहे मंत्रियों को हटाए
-
-
राजनीति के अपराधीकरण पर रोक
-
-
गंभीर आपराधिक आरोप झेल रहे मंत्रियों को पद पर बने रहने से रोकना
-
-
नौकरशाहों से तुलना
-
-
सिविल सेवकों को थोड़े समय की हिरासत पर निलंबित कर दिया जाता है
-
मंत्री, सार्वजनिक सेवक होने के नाते, उच्च मानक पर खरे उतरने चाहिए
-
-
जवाबदेही को बढ़ावा देना
-
-
30 दिनों का समय मंत्री के लिए जमानत पाने या कानूनी जवाब देने हेतु पर्याप्त है
-
आलोचनाएँ और चिंताएँ
-
‘दोष सिद्ध होने तक निर्दोष’ सिद्धांत का उल्लंघन
-
-
दोषसिद्धि नहीं, बल्कि हिरासत के आधार पर मंत्री हटाए जाते हैं
-
विधिक प्रक्रिया को कमजोर करता है
-
-
राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना
-
-
केंद्र द्वारा विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है
-
सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग हटाने के लिए किया जा सकता है
-
-
मनमाना हिरासत काल
-
-
30 दिन की सीमा सैद्धांतिक न होकर सामरिक लगती है
-
-
मौजूदा कानूनों से टकराव
-
-
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद होती है
-
लिली थॉमस केस और मनोज नारूला केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद अयोग्यता तय की; विधेयक इससे नीचे का मानक तय करता है
-
-
संघवाद के लिए खतरा
-
-
सत्ता का केंद्रीकरण, राज्य स्वायत्तता को कमजोर करना
-
-
नैतिक शासन बनाम लोकतांत्रिक सुरक्षा
-
-
समर्थक: यह सुप्रीम कोर्ट की पद पर ईमानदारी से जुड़ी टिप्पणियों से मेल खाता है
-
आलोचक: लोकतांत्रिक मानदंडों और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है
-
-
संभावित न्यायिक चुनौती
-
-
इसे बुनियादी ढाँचा सिद्धांत (कार्यपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण) के तहत परखा जा सकता है
-
मौजूदा ढाँचे से तुलना
-
धारा 8, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
-
-
विधायक केवल 2+ वर्ष की सजा पर दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित होते हैं
-
-
विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट
-
-
गंभीर अपराधों (5+ वर्ष) में आरोप तय होने के चरण से अयोग्यता सुझाई गई
-
पूर्व-दोषसिद्धि हिरासत पर कुछ नहीं कहा गया
-
-
सीमितता
-
-
वर्तमान कानूनों में जेल में रहकर भी मंत्री पद पर बने रह सकते हैं; विधेयक इस कमी को दूर करता है
-
संविधान संशोधन विधेयक
-
परिभाषा
-
-
संविधान में संशोधन हेतु विधायी प्रस्ताव, अनुच्छेद 368 के तहत
-
-
आवश्यकताएँ
-
-
विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 हिस्सा
-
यदि संघीय प्रावधान प्रभावित होते हैं तो आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन आवश्यक
-
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
-
उद्देश्य
-
-
जटिल या विवादास्पद विधेयकों की जांच करना
-
-
संरचना
-
-
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
-
सामान्यतः 31 सदस्य: 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा
-
-
कार्य
-
-
विधेयकों की धारा-दर-धारा समीक्षा
-
विशेषज्ञ राय लेना
-
संसद को सिफारिशी रिपोर्ट देना (बाध्यकारी नहीं)
-
निष्कर्ष
-
राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और संवैधानिक नैतिकता का समाधान करने का प्रयास
-
सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों में हिरासत में रहते हुए मंत्री पद पर न बने रहें
-
लेकिन यह विधिक प्रक्रिया, संघवाद और राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएँ उठाता है
-
दुरुपयोग से बचाव और संवैधानिक जांच इसके भविष्य को तय करेंगे