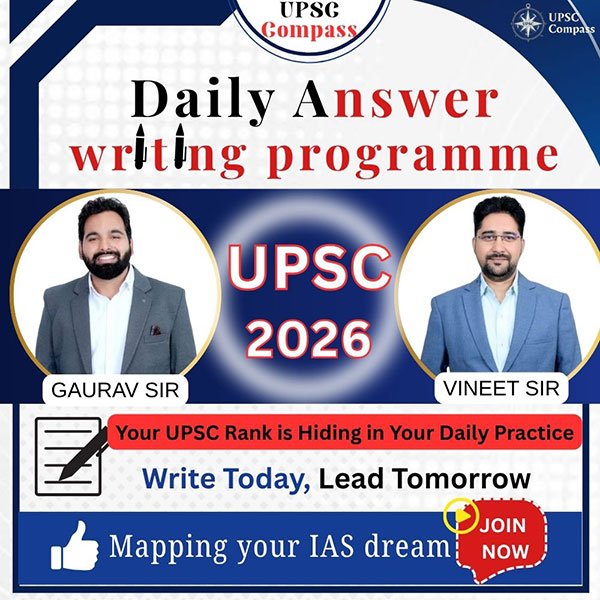समाचार में क्यों
-
नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट “Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta” जारी की।
-
यद्यपि रिपोर्ट का मुख्य फोकस दालों पर है, लेकिन इसमें बाजरा जैसी फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, जिनमें उत्पादकता, मूल्य निर्धारण और स्थिरता जैसी समान चुनौतियाँ हैं।
भारत में बाजरे की वर्तमान स्थिति और रुझान
उत्पादन हिस्सेदारी
-
भारत विश्व के लगभग 41 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन करता है।
-
वार्षिक उत्पादन लगभग 16 मिलियन टन है, जिससे भारत सबसे बड़ा उत्पादक है।
क्षेत्रीय एकाग्रता
-
80 प्रतिशत से अधिक बाजरे का उत्पादन कुछ ही राज्यों से आता है: राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
-
यह असमान भौगोलिक वितरण दर्शाता है।
खपत में गिरावट
-
प्रति व्यक्ति बाजरा खपत 1960 के दशक में 32 किलोग्राम प्रति वर्ष से घटकर आज केवल 4 किलोग्राम रह गई है।
-
सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आहार संबंधी बदलावों के कारण लोग चावल और गेहूँ की ओर चले गए।
निर्यात रुझान
-
भारत ने 2022–23 में लगभग 1.8 मिलियन टन बाजरे का निर्यात किया।
-
प्रमुख निर्यात गंतव्य: संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब।
-
वैश्विक मांग बढ़ने को दर्शाता है।
नीतिगत फोकस
-
केंद्रीय बजट 2023–24 में बाजरे का नाम बदलकर “श्री अन्न” रखा गया।
-
अनुसंधान, प्रसंस्करण और विपणन के लिए संसाधन आवंटित किए गए ताकि खपत को बढ़ावा दिया जा सके।
बाजरे का महत्व
पोषण मूल्य
-
लौह, कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर।
-
विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया से लड़ने में मदद करता है।
जलवायु सहनशीलता
-
चावल की तुलना में 70 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता।
-
सूखा और कमजोर मिट्टी सहने योग्य, वर्षा आधारित और शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
किसान आजीविका
-
कम निवेश वाली फसल, उर्वरकों और सिंचाई की कम आवश्यकता।
-
लघु और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत घटती है।
खाद्य सुरक्षा
-
मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल होने से कमजोर वर्गों के पोषण में सुधार।
वैश्विक मान्यता
-
भारत ने बाजरे को “श्री अन्न” के रूप में ब्रांड किया।
-
इसे सुपरफूड के रूप में विश्व स्तर पर प्रचारित किया, जिससे भारत की कृषि कूटनीति और निर्यात क्षमता मजबूत हुई।
अब तक उठाए गए कदम
-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (बाजरा): बीज वितरण, क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता सुधार का समर्थन।
-
श्री अन्न मिशन (2023): छह वर्ष का मिशन, अनुसंधान, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजरे को बाजार से जोड़ने के लिए।
-
राज्य योजनाओं में बाजरा: उदाहरण– कर्नाटक की “क्षीर भाग्य” योजना में स्कूल भोजन में बाजरा शामिल।
-
अंतर्राष्ट्रीय पहल: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जिसने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
-
निर्यात प्रोत्साहन: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ब्रांडिंग, भौगोलिक संकेत टैग और बाजरा आधारित निर्यात का समर्थन करता है।
बाजरे की चुनौतियाँ
उपभोक्ता पसंद में गिरावट
-
चावल और गेहूँ का प्रभुत्व, कारण– सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम कीमतें और आसान पकाना।
उत्पादकता अंतर
-
वर्तमान उत्पादकता लगभग 1.2 टन प्रति हेक्टेयर, जो चावल और गेहूँ से बहुत कम है।
-
अनुसंधान और बीज प्रणाली की कमजोरी इसका कारण।
बाजार संपर्क
-
किसानों को कमजोर मूल्य श्रृंखला, सीमित किसान उत्पादक संगठन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद की कमी का सामना करना पड़ता है।
फसल कटाई के बाद की समस्याएँ
-
खराब प्रसंस्करण तकनीक, भंडारण हानि और बाजरा आधारित उद्योगों में कम निवेश से मूल्य संवर्धन घटता है।
नीतिगत पक्षपात
-
चावल और गेहूँ के लिए सरकारी सब्सिडी वर्षा आधारित क्षेत्रों में बाजरे की खेती को हतोत्साहित करती है।
आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक ढाँचा
क्षैतिज विस्तार
-
विशेष रूप से पूर्वी भारत में धान की परती भूमि और अनुपजाऊ भूमि में बाजरे की खेती।
ऊर्ध्वाधर विस्तार
-
उच्च उत्पादकता वाले, जैव-संवर्धित और जलवायु सहनशील किस्मों का विकास।
-
बीज प्रणाली को मजबूत बनाना।
क्लस्टर आधारित मॉडल
-
जिलावार फसल क्लस्टर को बढ़ावा देना ताकि लक्षित हस्तक्षेप संभव हो।
मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण
-
प्रसंस्करण केंद्र, ब्रांडिंग इकाइयाँ और किसान उत्पादक संगठन आधारित एकत्रीकरण स्थापित करना।
जलवायु-स्मार्ट प्रथाएँ
-
जैविक खेती, जल-सक्षम पद्धतियों और कीट-प्रतिरोधी तकनीकों को प्रोत्साहित करना, ताकि भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हों।
आगे की राह
-
खाद्य सुरक्षा योजनाओं में एकीकरण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एकीकृत बाल विकास योजना में बाजरा शामिल करना अनिवार्य।
-
अनुसंधान और विकास को बढ़ावा: जैव-संवर्धित, कम अवधि वाली किस्मों और बीज प्रतिस्थापन में निवेश।
-
निर्यात केंद्रित मूल्य श्रृंखला: भौगोलिक संकेत आधारित ब्रांड और प्रीमियम बाजरा उत्पाद बनाना।
-
सार्वजनिक खरीद सुधार: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करना, विकेन्द्रीकृत केंद्रों के साथ।
-
जागरूकता अभियान: पोषण, जीवनशैली और जलवायु सहनशीलता से जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा प्रचार अभियान चलाना।
निष्कर्ष
-
बाजरा भारत को तीनहरी उपलब्धि देता है:
-
बेहतर पोषण
-
मजबूत जलवायु सहनशीलता
-
किसानों की आय में वृद्धि
-
-
मजबूत संस्थागत सहयोग, अनुसंधान और वैश्विक ब्रांडिंग के साथ, बाजरा भविष्य का अनाज बन सकता है।
-
आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उत्पादन, बाजार और उपभोक्ता जागरूकता सभी स्तरों पर संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं।