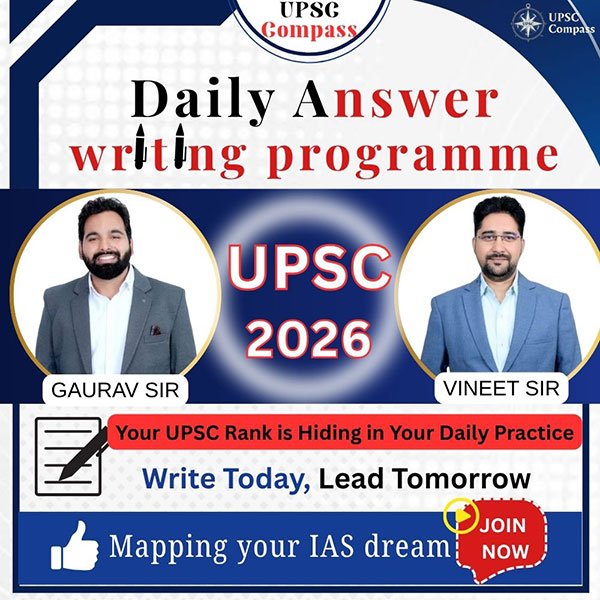समाचार में क्यों
-
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने भारत के साइबरस्पेस ऑपरेशंस और एंफिबियस ऑपरेशंस के संयुक्त सिद्धांत (जॉइंट डॉक्ट्रिन्स) को डीक्लासिफाई कर जारी किया है।
-
उद्देश्य
-
इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना
-
राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को मजबूत करना
-
एकीकृत मल्टी-डोमेन युद्ध के लिए मार्गदर्शन देना
-
साइबरस्पेस ऑपरेशंस के बारे में
-
साइबरस्पेस क्या है?
-
-
एक वैश्विक क्षेत्र जिसमें आपस में जुड़े सिस्टम, नेटवर्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जैसे:
-
इंटरनेट
-
इंट्रानेट्स
-
कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स
-
कंट्रोल सिस्टम
-
-
यह एक महत्वपूर्ण वातावरण के रूप में कार्य करता है:
-
जानकारी बनाने के लिए
-
जानकारी प्रसारित करने के लिए
-
जानकारी को बदलने (मैनिपुलेट) के लिए
-
जानकारी को संग्रहीत करने के लिए
-
-
-
साइबरस्पेस की विशेषताएं
-
-
सीमाहीन क्षेत्र – भौगोलिक सीमाओं से परे
-
द्वि-उपयोग प्रकृति – नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति
-
वास्तविक समय प्रभाव – क्रियाओं का तत्काल वैश्विक असर
-
गुमनामी और एट्रिब्यूशन चुनौतियां – कारकों का पता लगाना कठिन
-
लगातार विकसित होते खतरे – तकनीकी बदलाव के साथ अनुकूलित
-
-
साइबरस्पेस ऑपरेशंस के घटक
-
-
डिफेंसिव साइबर ऑपरेशंस – नेटवर्क को हैकिंग, मालवेयर और डेटा चोरी से बचाना
-
ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस – दुश्मन के सिस्टम में घुसपैठ कर संचार को बाधित करना और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना
-
साइबर इंटेलिजेंस और रिकॉनसेंस – कमजोरियों की पहचान, हमलों का पूर्वानुमान और योजना में सहायता
-
साइबर सपोर्ट ऑपरेशंस – थल, वायु, समुद्री और अंतरिक्ष अभियानों के लिए तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना
-
रेजिलियंस और रिकवरी सिस्टम – संकट के समय बैकअप और त्वरित बहाली की व्यवस्था
-
-
संचालन के सिद्धांत
-
-
सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित खतरे-केंद्रित योजना
-
सशस्त्र सेवाओं और नागरिक एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी
-
कई सुरक्षा अवरोधों का उपयोग करके लेयर्ड डिफेंस
-
घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत कानूनी और नैतिक अनुपालन
-
नुकसान को कम करने के लिए वास्तविक समय प्रतिक्रिया
-
एंफिबियस ऑपरेशंस के बारे में
-
एंफिबियस ऑपरेशंस क्या हैं?
-
-
समुद्र से नौसेना, वायुसेना और थल सेना द्वारा शुरू किए गए समन्वित सैन्य अभियान, ताकि तट पर मिशन पूरा किया जा सके
-
इनका उपयोग:
-
युद्ध
-
मानवीय सहायता
-
आपदा राहत (HADR)
-
विवादित क्षेत्रों में बल प्रदर्शन
-
-
-
एंफिबियस ऑपरेशंस की विशेषताएं
-
-
त्रि-सेवा एकीकरण – नौसेना, वायु और थल बलों का संयोजन
-
त्वरित प्रतिक्रिया – समुद्र से तट तक तेज़ तैनाती
-
लचीले मिशन प्रोफाइल – युद्ध से लेकर HADR तक
-
रणनीतिक पहुंच – द्वीपों और तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव
-
समुद्री-स्थलीय संबंध – समुद्र आधारित क्षमताओं को स्थलीय उद्देश्यों से जोड़ना
-
सिद्धांतों का महत्व
-
राष्ट्रीय सुरक्षा – पावर ग्रिड, रक्षा नेटवर्क और संचार जैसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर की रक्षा
-
फोर्स मल्टीप्लायर – पारंपरिक युद्ध रणनीतियों के साथ साइबर उपकरणों का एकीकरण
-
समुद्री श्रेष्ठता – लिटोरल ज़ोन में प्रभुत्व सुनिश्चित करना
-
सशस्त्र बलों में संयुक्तता – थल, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना
-
हाइब्रिड युद्ध तैयारी – संयुक्त साइबर, समुद्री और थल खतरों का सामना करना
-
कूटनीतिक संदेश – भारत की क्षमता और संकल्प का प्रदर्शन
निष्कर्ष
-
ये डीक्लासिफाइड सिद्धांत भारत की रक्षा तैयारियों में एक रणनीतिक छलांग को दर्शाते हैं
-
त्रि-सेवा एकीकरण को मजबूत करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और मल्टी-डोमेन संघर्षों के लिए तत्परता बढ़ाना